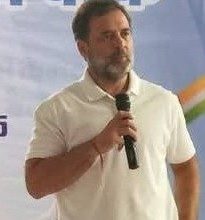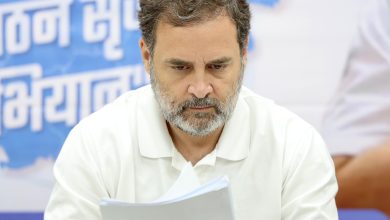Editorial
जनगणना और जातिगत आधार

संसद में जातिगत जनगणना का मामला फिर से उठने लगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामला उठाया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति को लेकर फब्ती कसना शुरू कर दिया। हालांकि यह बहस गलत दिशा में जाती दिख रही है, लेकिन जनगणना तो होना ही है। इसमें यदि जाति का मुद्दा शामिल कर लिया जाए तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज टिकट वितरण से लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति तक राजनीतिक दलों में अधिकांश जातिगत आधार पर ही होती है। फिर जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है?
जनगणना की बात करें तो भारत में उन्नीसवीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था। उसके पीछे संभवत: इस विशाल देश पर शासन करना आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन बाद में दशकीय-जनगणना इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और कई विद्वानों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जनगणना के आंकड़ों से ही हमें लगभग 50 साल पहले भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या का पता चला, लडक़ों की तुलना में लड़कियों की उच्च मृत्यु दर। 1881 से 2011 तक, हर दस साल में प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में जनगणना की जाती थी। इसके अनुसार अगली जनगणना 2021 में होनी थी।
कोविड संकट ने केंद्र सरकार को जनगणना स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया। तब से तीन साल बीत चुके हैं, और अगली जनगणना के लिए अभी भी सक्रिय तैयारी का कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि सौ से अधिक देशों ने कोविड के दौरान या उसके बाद जनगणना की है। जनगणना में देरी से स्वाभाविक तौर पर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे कि हम 2011 के बाद से साक्षरता की प्रगति का आकलन करने में असमर्थ हैं। कोविड के दौरान लगभग दो साल स्कूल बंद रहे, हमें यह जानने की जरूरत है कि इससे बच्चों की पढऩे-लिखने की क्षमता पर क्या असर पड़ा। जनगणना कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे, यह प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी का स्रोत है। राज्यों के बीच कर-राजस्व के आवंटन के लिए इसकी जरूरत है। इसका उपयोग कई सर्वेक्षणों के लिए एक रूपरेखा के रूप में किया जाता है। कई मुद्दों पर तो अंदाज से ही काम चलाया जा रहा है।
जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता का एक और कारण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का न्यूनतम कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 2013 में अधिनियम के लागू होने के बाद ये अनुपात 2011 की आबादी पर लागू किए गए और 80 करोड़ व्यक्ति सस्ते अनाज के हकदार बने। यदि वही अनुपात वर्तमान आबादी पर लागू किए जाते तो शायद आज अन्य 10 करोड़ लोग सस्ते अनाज से लाभान्वित होते। आज लगभग 10 करोड़ लोग जन-वितरण प्रणाली से वंचित हैं, क्योंकि सरकार पुरानी जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रही है।
जनगणना के साथ ही परिसीमन भी होना है। लेकिन बिना जनगणना के परिसीमन का कोई औचित्य ही नहीं होगा। भारत के उत्तरी राज्यों की आबादी दक्षिणी राज्यों की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। इसलिए आबादी में उत्तरी राज्यों का हिस्सा आज 1973 की तुलना में ज्यादा है। हालांकि आज की परिस्थितियों में परिसीमन सत्ता पर काबिज भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में सीटों की संख्या दक्षिण के मुकाबले काफी अधिक बढ़ जाएंगी और वहां भाजपा का वोट प्रतिशत अधिक है।
अब आते हैं जातिगत जनगणना पर। बिहार का मामला अभी सामने आया। हालांकि वहां की जातिगत जनगणना से कई जातियों को नुकसान भी होने की आशंका है, लेकिन हमें इसका सही आंकड़ा तो मालूम होना ही चाहिए कि कहां किस जाति के कितने लोग रहते हैं। देखा जाए तो भले ही कई राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि वे जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करतीं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जब टिकट बांटे जाते हैं, तो पूरे भले ही नहीं, लेकिन जातिगत वोटरों का अनुपात तो देखा ही जाता है। औसत भी देखा जाता है। और फिर जातिगत संतुलन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।
विधानसभा और लोकसभा सीटों का आरक्षण भी अनुसूचित जाति, जनजाति के आधार पर जब होता है, तो इसमें सभी जातियों की आबादी सार्वजनिक करने में क्या समस्या है? संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर भले ही बहस गलत दिशा में चली गई हो, लेकिन जब पूरी राजनीति जाति आधारित हो रही है, तो जनगणना के दौरान जाति की आबादी स्पष्ट करने में क्या हर्ज है? संसद की बहस तो गलत दिशा में जाती दिख रही है। जो सवाल केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष से पूछ रहे हैं, यदि यही सवाल कांग्रेस सांसद पूछते तो निश्चित तौर पर दर्जनों एफआईआर दर्ज करवा दी जातीं और अदालतों में याचिकाओं की कतार लग जाती। यह उचित बहस नहीं कही जा सकती। लेकिन जनगणना का मौका आ गया है, तो जनगणना का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए।
– संजय सक्सेना