-
Lifestyle

-
Latest News

-
State

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
मध्य प्रदेश

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News
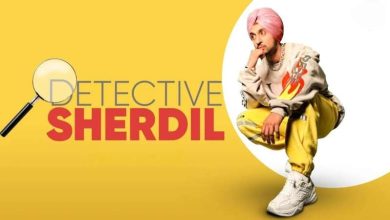
-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News
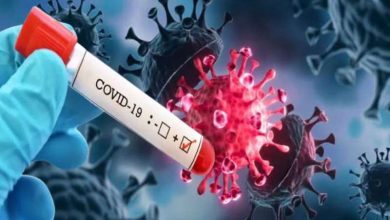
-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News
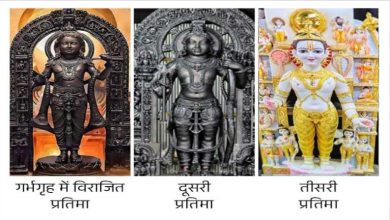
-
Latest News
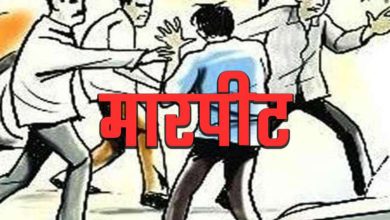
-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

-
Latest News

